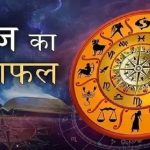लखनऊ, 20 फरवरी 2024 : लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मेरे एक मित्र अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में काम करते हैं। उन्होंने एक बार बताया कि एक ब्लॉक स्तर के अधिकारी ने उनसे पहली मुलाक़ात और बातचीत के बाद ही उन्हें अपने बेटे की शादी में आमंत्रित कर दिया। मैंने जब हैरानी जताते हुए इसका कारण पूछा तो पता चला कि वे अधिकारी मेरे मित्र के बातचीत के ढंग से पहचान गए कि वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ से स्वयं वे अधिकारी भी थे।
यह क़िस्सा हमें बताता है कि भाषा सिर्फ़ भाषा नहीं होती, वह एक संस्कृति होती है, अस्तित्व की पहचान होती है जो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अक़्सर हम ऐसे लोगों से टकराते हैं जो आसानी से किसी के बातचीत के ढंग से उसके मूल निवास का पता लगा लेते हैं। अवचेतन रूप से हम सभी अपनी मूल भाषा-संस्कृति को अपने साथ लेकर चलते हैं और चाहे-अनचाहे वह हमारे व्यवहार में प्रदर्शित हो जाती है। भाषा वह कड़ी होती है जो किसी भी देश, राज्य या शहर में हमें एक-दूसरे से जोड़ती है।
21 फरवरी-अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हम सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि बचपन से लेकर जीवनभर हम जो कुछ भी सीख रहे होते हैं, उसका आधार भाषा ही है। हमारा सोचना, तर्क करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, अपनी बात को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना, ये सभी भाषा के माध्यम से ही हो पाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे सोचने में, हमारे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण (Intrapersonal Communication) में, दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए में कौन-सी भाषा होती है? हम कई भाषाओं के जानकार हो सकते हैं, कई भाषाओं को ना सिर्फ़ बोल सकते हैं बल्कि उन्हें पढ़ना और लिखना भी हमें आता है परंतु अवचेतन रूप में सोचने-विचारने या दुनिया को देखने के नज़रिए में हममें से ज़्यादातर लोग अपनी उस भाषा को ही काम में लेते हैं जिसे हमने स्कूल जाने से पहले अर्जित किया होता है।
भाषा के इस रूप और ऐसे महत्व को अक्सर औपचारिक शिक्षा में नकार दिया जाता है और यही कारण है कि देश में 1369 मातृभाषाएँ होने के बावजूद मात्र 22 भाषाएँ ही भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं। केवल 28 भाषाएँ ही बतौर ‘शिक्षण का माध्यम’ इस्तेमाल की जाती हैं और दस लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली 33 भाषाओं को ‘शिक्षण का माध्यम’ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। सीखने में भाषाओं (मातृभाषाओं) के महत्व को नकारने का परिणाम ये है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आज भी देश के लगभग 30 प्रतिशत बच्चे सीखने में मध्यम से गंभीर स्तर की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारतीय संविधान से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तक में मातृभाषा/घर की भाषा को ‘शिक्षा का माध्यम’ बनाने की बात कही गई है। इसके बावजूद बच्चों की भाषा को औपचारिक शिक्षा में शामिल करने में कई बाधाएँ हैं।
विभिन्न भाषाओं को सामाजिक स्तर के अनुसार दर्जा देना पहली बाधा है जहाँ किसी विशेष भाषा को उच्च स्तर पर रखा जाता है जबकि कुछ भाषाओं, विशेषकर जनजातीय भाषाओं, को निम्न माना जाता है। इसके अलावा हमारी पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें यह मानकर तैयार की जाती हैं कि बच्चे स्कूल की भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं और वे आराम से उस भाषा में बात कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में बच्चों की प्रथम भाषा को कमतर और कक्षा में इस्तेमाल के लायक नहीं समझा जाता है। ये सभी बातें मिलकर औपचारिक शिक्षा को उन बच्चों के लिए दूभर बना देती हैं जिनकी भाषा सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर रखी गई भाषा से अलग होती है जबकि ये बच्चे अपनी भाषा में वे सारे काम कर रहे होते हैं जो वास्तव में जीवन के लिए ज़रूरी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम सभी को भाषा के वृहत् रूप को पहचानने और उसे अपनाने की आवश्यकता है जिससे भाषा-भाषा में किसी भी प्रकार का भेद ना रहे और हमारा भविष्य भाषा संबंधित पूर्वाग्रहों के कारण आगे बढ़ने से ना रुके।
- स्मृति मिश्रा,
लेखिका वर्तमान में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, नई दिल्ली में बहुभाषी शिक्षा इकाई में कार्यरत हैं।