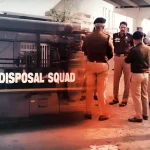राधिका कालिया, एमडी, आरएलजी सिस्टम्स इंडिया
आधुनिक समय ने हमें “मूल्य” अथवा “वैल्यू” के नए आयाम, दृष्टिकोण, नयी परिभाषाएं और अवधारणाएं प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए आज कचरे को भी एक संसाधन की तरह देखा और प्रयोग किया जाने लगा है। आज विभिन्न प्रकार के कचरे का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) कर के उसको दोबारा से अर्थव्यवस्था में संचारित करने पर बल दिया जाने लगा है। विशेष कर इलेक्ट्रॉनिक कचरे या ई-वेस्ट को “वैल्यू” के महत्वपूर्ण स्त्रोत की दृष्टि से देखा जाने लगा है। आज ई-वेस्ट केवल टूटे-फूटे उपकरणों का ढेर नहीं रहा, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है। हालांकि यह भी ध्यातव्य है और विडम्बना सी लग सकती है कि तकनीकी उन्नति के चलते जो सुविधा प्रदान हुई है और जो पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हुआ है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हाल ही में मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 23 करोड़ रुपये मूल्य का अवैध ई-वेस्ट जब्त किया; इसमें 17,000 से अधिक लैपटॉप, 11,000 से अधिक सीपीयू और हज़ारों चिप्स सम्मिलित हैं जो ‘एल्यूमिनियम स्क्रैप’ के नाम पर छिपाकर लाए गए थे। यह घटना इस ओर संकेत करती है कि जैसे-जैसे वस्तुओं के मूल्य की धारणा बदलती है, वैसे-वैसे व्यापारिक व्यवहार भी बदल जाते हैं — चाहे वे कानूनी हों या अवैध। जब किसी वस्तु को, चाहे वह कचरा ही क्यों न हो, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी या लाभदायक माना जाने लगता है, तो वह बाज़ार की गतिविधियों का हिस्सा बन जाती है। किसी वस्तु का अवैध व्यापार में शामिल होना इस बात का संकेत है कि उसका प्रभाव और महत्व अर्थव्यवस्था में बढ़ चुका है, और जब किसी संसाधन का मूल्य बढ़ता है, तो उसके नियमन और नियंत्रण के नियम भी नए रूप लेते हैं। यह सत्य है कि आज ई-वेस्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, और ई-वेस्ट का मूल्य इतना है कि अब इसका अवैध व्यापार आकर्षक हो गया है।
परंतु किसी भी व्यवस्था की वास्तविक शक्ति उसके नियमों में नहीं, बल्कि उस विश्वास और सम्मान में निहित होती है जो समाज उन नियमों के प्रति रखता है। जब आचरण और आस्था साथ चलते हैं, तभी नीति व्यवस्था बनती है, और वही किसी राष्ट्र की स्थायी शक्ति का आधार होती है। भारत ने ‘ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022’ और ‘एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर)’ जैसी नीतियों के माध्यम से दिशा तय कर दी है, पर वास्तविक सफलता तब होगी जब इन नियमों का भाव नागरिक चेतना का हिस्सा बनेगा। उदाहरणस्वरूप, बैटरी अपशिष्ट (विशेषकर लिथियम-आधारित) व्यापक ई-वेस्ट समस्या का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। आरएलजी सिस्टम्स इंडिया जैसी कंपनियां उत्पादकों को लिथियम बैटरी कचरे के जिम्मेदार संग्रहण और पुनर्चक्रण में सक्षम बनाकर उनकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) दायित्वों को पूरा करने में सहयोग देती हैं, किन्तु कानून केवल सीमाएँ तय करता है, और संवेदना ही अनुशासन को संस्कार में बदलती है। ई-वेस्ट नीति का असली उद्देश्य यही है कि तकनीकी विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक-दूसरे के पूरक बनें, विरोधी नहीं।
दिल्ली के होलम्बी कलां में बन रहा ई-वेस्ट पार्क इसका उत्तर खोजने की दिशा में एक ठोस कदम है। नॉर्वे की रेवाक (Revac) सुविधा से प्रेरित यह परियोजना “जीरो-वेस्ट” सिद्धांत पर आधारित है — न जलाना, न प्रदूषण, न अपशिष्ट उत्सर्जन। इसकी क्षमता अब बढ़ाकर 1.1 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है, जो बताती है कि भारत अब केवल नीति नहीं, संरचना भी बना रहा है। यह बड़ा संकेत है कि पर्यावरण अब मंत्रालय का विषय नहीं, उद्योग नीति का हिस्सा बन रहा है। उधर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नागरिकों से सीधे ई-वेस्ट एकत्र करने के लिए भुगतान-आधारित प्रणाली शुरू कर रहा है, और आंध्र प्रदेश के ओंगोल नगर निगम ने अपने पहले 3.72 टन ई-वेस्ट को अधिकृत रीसाइक्लर को भेज दिया है। ये पहलें दर्शाती हैं कि भारत में अब राज्य अपने मॉडल स्वयं गढ़ रहे हैं।
यहां यह दोहराना उचित होगा कि ई-वेस्ट केवल नीति का नहीं, संस्कार का भी प्रश्न है। जब तक उपभोक्ता अपने पुराने उपकरणों को जिम्मेदारी से नहीं लौटाते, तब तक न तो कोई सिस्टम प्रभावी होगा, न ही कानून से अपेक्षित परिणाम आएंगे। “मरम्मत करो, पुनः-उपयोग करो, लौटाओ” (रिपेयर, रीयूज एंड रीसायकल) नागरिक अनुशासन का नया सूत्र बनना चाहिए। आज अधिकतर लोग नया खरीदना सुविधा मानते हैं, लेकिन भविष्य में रीसायकल-संस्कृति ही भारत की परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) की नींव बनेगी।
ई-वेस्ट का दूसरा आयाम रणनीतिक है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन और ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे धातु अत्यंत आवश्यक हैं। यही तत्व पुरानी बैटरियों, मोबाइल-चिप्स और लैपटॉप में छिपे हैं। जब केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने देश-व्यापी ई-वेस्ट संग्रह अभियान शुरू किया, तो उसका उद्देश्य केवल सफाई नहीं था — वह भारत को खनिज-स्वराज्य की ओर ले जाने का प्रयास था।
हर पुराना उपकरण अब “मिनी-माइन” है, और हर रीसाइक्लिंग यूनिट “नई खान”। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का नॉर्वे दौरा हो या कानून और न्याय मंत्रालय का स्वयं अपने पुराने कंप्यूटरों को सूचीबद्ध कर अधिकृत रीसाइक्लर को भेजना, ये घटनाएँ बताती हैं कि सरकार अब उदाहरण प्रस्तुत करने के स्तर पर सोच रही है और जन-सामान्य में जागरूकता और चेतना का विकास करने का प्रयास कर रही है। शासन तभी प्रभावी बनता है जब वह अपने आचरण से नीति को जीवंत करे।
“वैल्यू” की नवीन अवधारणा विकास के लिए उत्पादन के साथ पुनरुत्पादन पर भी बल देती है। हालांकि भारत की संस्कृति और व्यवहार में बचत और पुनर्प्रयोग तो प्राचीन काल से अन्तर्निहित हैं, तथापि कचरे को संसाधन में बदलने की यह यात्रा केवल पर्यावरण नीति नहीं, औद्योगिक नैतिकता का पुनर्लेखन है। इसी संस्कार को अपनी रोज़मर्रा के जीवन में निहित करके भारत पुनरुपयोग-प्रधान राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर हो सकता है।