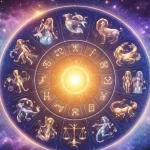बाय एकता खुराना, साइकोलॉजिस्ट
जैसे-जैसे हर साल यह दिन आता है, विश्व वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेकर चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं। लेकिन क्या साल में एक दिन तंबाकू से दूर रहने की कसम खाना उस लत को खत्म करने के लिए काफी है, जो इंसानी मन में गहराई तक घर कर चुकी है? तंबाकू छोड़ने की कोशिश को सिर्फ प्रतीकात्मक दिवस तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सालभर चलने वाले जनआंदोलन का रूप देना होगा।
साथ ही, तंबाकू के आदी लोगों को ऐसे व्यावहारिक विकल्प भी दिए जाने चाहिए जो नुकसान कम करने में मदद करें – बजाय इसके कि उन्हें जबरन तंबाकू छोड़ने पर मजबूर किया जाए, जो अक्सर असफल ही होता है।
भारत में तंबाकू का सेवन – बल्कि कहें तो इसकी लत – एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। इसकी वजहें केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी हैं, जो अलग-अलग आयु और वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं।
हालांकि तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए अब तक कई पहल की गई हैं, लेकिन उनका असर अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा है। इसलिए अब ज़रूरत है कि इस समस्या को एक नए नज़रिए से समझा जाए। तंबाकू की लत के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई से पड़ताल की जाए और फिर उसी आधार पर ऐसी रणनीतियां तैयार की जाएं, जो वाकई असर दिखाएं।
*मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ तम्बाकू नियंत्रण रिपोर्ट
तनाव और चिंता – तंबाकू की लत के प्रमुख कारण
भारत में तंबाकू की लत के पीछे सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक कारणों में तनाव और चिंता शामिल हैं। कई लोग कामकाज, पारिवारिक समस्याओं या निजी जीवन की उलझनों से पैदा होने वाले तनाव से राहत पाने के लिए धूम्रपान या तंबाकू चबाने का सहारा लेते हैं।
तंबाकू में मौजूद निकोटिन एक तेज़ उत्तेजक होता है, जो थोड़ी देर के लिए तनाव और बेचैनी से राहत जरूर देता है, लेकिन यह कभी स्थायी समाधान नहीं बन सकता।
‘ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल’ रिपोर्ट में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, टीयर-1 शहरों में 62% पुरुष और 40% महिलाएं तनाव और चिंता से निपटने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं।
साथियों का दबाव और सामाजिक स्वीकृति – शौक से लत तक का सफर
तंबाकू की आदत में पड़ने का एक और बड़ा कारण है सामाजिक दबाव और तथाकथित ‘कूल’ दिखने की चाह। कई बार लोग सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कदम मिलाने या “भीड़ में फिट होने” के लिए तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। यह आदत धीरे-धीरे एक लत का रूप ले लेती है।
विभिन्न शोधों में यह बात सामने आई है कि साथियों के दबाव के कारण ही युवा तंबाकू आजमाते हैं, और फिर इसका नियमित सेवन शुरू हो जाता है। यह प्रवृत्ति शहरों के साथ-साथ गांवों के युवाओं में भी समान रूप से देखी गई है।
संवेदनशीलता और मनोवैज्ञानिक मजबूती की कमी – एक क्षणिक संतुष्टि जो कभी टिकती नहीं
आज की दुनिया में, जहां तात्कालिक संतुष्टि से जुड़ी डोपामाइन की लहर लोगों को तेजी से लुभा रही है, वहीं आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए धूम्रपान का सहारा लेने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यह व्यवहार अक्सर बहुत ही कम आत्मसम्मान, किसी पुराने आघात के अनुभव, आवेग में की गई प्रतिक्रियाओं या सनसनी की तलाश जैसी मानसिक अवस्थाओं का परिणाम होता है।
ये कारण, चाहे अकेले हों या मिलकर असर डालें, लोगों को तंबाकू में एक तात्कालिक राहत की झूठी उम्मीद दिखाते हैं – लेकिन यह राहत न तो स्थायी होती है और न ही लाभकारी।
भूख को दबाने का बहाना – वंचित तबकों में तंबाकू की लत का खतरनाक भ्रम
‘ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कानूनी रूप से बनने वाली सिगरेटें कुल तंबाकू खपत का सिर्फ 8% हिस्सा हैं, जबकि बीड़ी, खैनी और चबाने वाली तंबाकू जैसे सस्ते विकल्प 92% हिस्सेदारी रखते हैं।
करीब 70 करोड़ भारतीय आज भी किसी न किसी रूप में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यह गलत धारणा फैल गई है कि तंबाकू भूख को दबा सकती है – और यही सोच वंचित समुदायों को इसकी लत में धकेल रही है।
यह एक भ्रामक सोच है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उल्टा, यह आदत समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है।
इससे उन समुदायों में तंबाकू छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, जहां धूम्रपान और जीवन के बुनियादी संघर्ष एक-दूसरे से गहराई से जुड़े नजर आते हैं – भले ही यह जुड़ाव केवल धारणा का हिस्सा हो।
चुनौती का समाधान – शुरुआत में ही रोकथाम जरूरी
भारत में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों में केवल नीति और प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि समझ, सहानुभूति और मानव केंद्रित सोच को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक वजहों को भी गहराई से समझना और उनका समाधान करना जरूरी है। इस दिशा में
अपनाई जाने वाली रणनीति में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए:
• ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाना जो तंबाकू के नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाएं और तनाव व चिंता से निपटने के लिए सुरक्षित और स्वस्थ विकल्पों के बारे में लोगों को समझाएं।
• तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक, तंबाकू उत्पादों पर अधिक कर और इनके उत्पादन व बिक्री पर सख्त नियंत्रण जैसे प्रावधानों के ज़रिए तंबाकू नियंत्रण नीतियों को और मज़बूत बनाना।
• विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तंबाकू छोड़ने की सुविधाओं को सुलभ और सस्ती बनाते हुए इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनाना।
विकल्प, जागरूकता और आसान पहुंच के साथ – एक दीर्घकालिक समाधान की ओर
तंबाकू की समस्या से निपटने के प्रयास तभी असरदार होंगे जब इसके पीछे छिपे कारणों को गहराई से समझा जाए और उन्हें जड़ से समाप्त करने की कोशिश की जाए। इसके लिए एक ऐसी समन्वित रणनीति की जरूरत है जो तंबाकू की लत के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को स्वीकार कर उनका समाधान करे।
इसके बाद शिक्षा, जन-जागरूकता, सशक्त नीतिगत सुधारों और समुदाय आधारित पहलों को इसमें जोड़ा जाना चाहिए।
मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि तंबाकू की लत से जूझ रहे लोगों को समझदारी और सहानुभूति के साथ ऐसा रास्ता दिखाया जाए, जिससे वे धीरे-धीरे एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें।
ऐसे में निकोटीन गम, पैच, लोजेंजेस और अन्य तकनीकी उपायों के विकल्पों की जानकारी और इन तक आसान पहुंच बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि तंबाकू छोड़ने की इस लड़ाई को गति मिल सके और एक स्वस्थ एवं सुरक्षित भारत की ओर बड़ा कदम बढ़ाया जा सके।